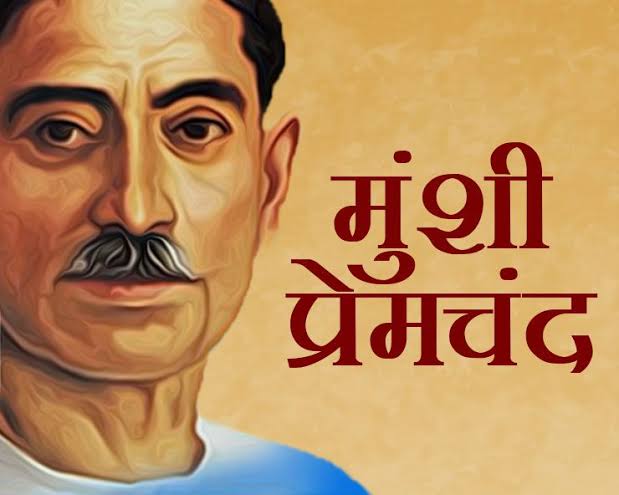आधुनिक हिंदी साहित्य के शिखर पुरुष एवं उपन्यास सम्राट मुंशी प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक थे। वह एक कुशल वक्ता, संवेदनशील लेखक, सचेत नागरिक एवं विद्वान संपादक थे। हिंदी साहित्य में उन्होंने यथार्थवादी परंपरा की शुरुआत की। जिस परंपरा की उन्होंने शुरुआत कि उसने आगे चलकर हिंदी साहित्य का मार्गदर्शन किया। प्रेमचंद का बचपन काफी आर्थिक बदहाली में गुजरा। भयंकर गरीबी के बावजूद भी उनकी लेखन के प्रति रुचि कम नहीं हुई। 13 वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने लेखन कार्य आरंभ कर दिया था। उनके पिता ने 15 वर्ष की आयु में ही उनकी शादी उनकी उम्र से अधिक और बदसूरत लड़की के साथ करवा दी थी। इससे वह दु:खी भी हुए। उन्हें लगातार अपने जीवन में विषम परिस्थितियों का सामना करना पड़ा। पिता के देहांत के बाद अचानक उनके सर पर पूरे घर का बोझ आ गया। उनकी आर्थिक बदहाली का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि पैसे के अभाव में उन्हें अपना कोट और पुस्तकें बेचनी पड़ी। अपनी गरीबी और जीवन के प्रतिकूल परिस्थितियों से जूझते हुए जैसे-तैसे शिक्षा प्राप्त की। परंतु प्रतिकूल परिस्थितियां भी प्रेमचंद के साहित्य-प्रेम को नहीं रोक सकी। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के बहुत बड़े विद्वान थे। सादा एवं सरल जीवन के मालिक प्रेमचंद ने यथार्थ पर आधारित कई कहानियां, नाटक, उपन्यास एवं लघु कथाएं लिखी। प्रेमचंद की रचना-दृष्टि विभिन्न साहित्य के रूप में प्रवृत हुई। बहुमुखी प्रतिभा के धनी प्रेमचंद ने कुल 15 उपन्यास, 300 से अधिक कहानियां, 3 नाटक, 10 अनुवाद, 7 बाल पुस्तक तथा हजारों लेख, संपादकीय, पत्र आदि की रचना की, परंतु उन्हें प्रसिद्धि और प्रतिष्ठा उपन्यास और कहानियों से प्राप्त हुई। प्रसिद्ध बंगाली लेखक शरद चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट की उपाधि दी। एक बार मुंशी प्रेमचंद से उनके समकालीन पत्रकार बनारसी दास चतुर्वेदी ने 1930 ईस्वी में उनके प्रिय रचनाओं के बारे में प्रश्न किया। उन्होंने पूछा कि आपकी सर्वोत्तम 15 गल्पें कौन सी हैं? प्रेमचंद ने उत्तर दिया,” इस प्रश्न का जवाब देना कठिन है, 200 से ऊपर गल्पों में कहां से चुनू?, लेकिन स्मृति से काम ले कर लिखता हूं।” उन्होंने जिस 15 रचनाओं की चर्चा की, वे थे- 1. बड़े घर की बेटी, 2. रानी सारन्धा, 3. नमक का दारोगा, 4. सौत, 5. आभूषण, 6. प्रायश्चित, 7. कामना, 8. मंदिर और मस्जिद, 9. घांसवाली, 10. महातीर्थ, 11. सत्याग्रह, 12. लांछन, 13. सती, 14. लैला, और 15. मंत्र। उनकी पहली रचना शोजेवतन (राष्ट्र का विलाप) 1908 में प्रकाशित हुई जो उनका पहला कहानी संग्रह था। जिसमें उन्होंने देश के तत्कालीन समस्याओं एवं दुख-दर्द का चित्रण किया। शोजेवतन के अतिरिक्त उनके प्रमुख कहानी संग्रह में ‘सप्त सरोज’, ‘नव निधि’, ‘प्रेम पूर्णिमा’, ‘प्रेम पच्चीसी’, ‘प्रेम प्रतिमा’, ‘प्रेम द्वादशी’, ‘समर यात्रा’ और ‘मानसरोवर’ आदि प्रमुख है। उनकी कहानियों में विषय और शिल्प की विविधता होती है। उन्होंने मनुष्य के सभी वर्गों से लेकर पशु-पक्षियों तक को अपनी कहानियों में मुख्य पात्र के रूप में प्रस्तुत किया है। उनकी कहानियां किसानों, मजदूरों, स्त्रियों, दलितों आदि की समस्याओं पर आधारित होती है। उन्होंने समाज-सुधार, देश-प्रेम, स्वाधीनता संग्राम आदि से संबंधित कहानियां भी लिखी है। प्रेमचंद की प्रमुख कहानियों में ‘पंच परमेश्वर’, ‘दो बैलों की कथा’, ‘ईदगाह’, ‘बड़े घर की बेटी’, ‘पूस की रात’, ‘कफन’, ‘गुल्ली-डंडा’, ‘ठाकुर का कुआं’, ‘बूढ़ी काकी’, ‘दूध का दाम’, ‘सद्गति’, ‘नमक का दारोगा’, ‘घासवाली’, ‘सत्याग्रह’ आदि का प्रमुखता से नाम लिया जा सकता है। उनकी कहानियों में समाज में फैली कुरीतियों पर जबरदस्त कुठाराघात किया गया है। प्रेमचंद की कहानियां समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए मार्गदर्शन का काम करती है।
‘नमक का दारोगा’ एक ईमानदार नमक निरीक्षक की कहानी है जिसने कालाबाजारी के विरुद्ध आवाज उठाई। इस कहानी में मानव मूल्यों का आदर्श रूप प्रस्तुत किया गया है। साथ ही सत्य-निष्ठा, धर्म-निष्ठा और कर्म परायणता को प्रदर्शित किया गया। कहानी का नायक मुंशी वंशीधर है, जिनकी नौकरी नमक के दारोगा के पद पर हो जाती है। कहानी में पंडित अलोपीदीन जो कि एक जमींदार हैं और नमक का व्यापार करता है, उसने अवैध रूप से नमक ले जाने के लिए दारोगा जी को घूस देने का प्रयास करता है, लेकिन दारोगा मुंशी वंशीधर अपने कर्म परायणता और धर्म निष्ठा से विमुख नहीं होते और ईमानदारी का परिचय देते हुए पंडित अलोपीदीन को गिरफ्तार कर लिया। कोर्ट में केस चला, धन और बल के बदौलत पंडित अलोपीदीन बरी हो गए। अगले दिन मुंशी वंशीधर को ईमानदारी का पुरस्कार मिला और उन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। बाद में पंडित अलोपीदीन ने वंशीधर की इमानदारी से प्रभावित होकर अपनी सारी जायदाद आजीवन मैनेजर बना दिया। यह कहानी सत्य निष्ठा, धर्म निष्ठा और कर्म परायणता के दुर्लभ गुणों का बखान करता है।
कहानी ‘बड़े घर की बेटी’ में यह बताने की कोशिश की गई है कि एक स्त्री किस प्रकार से अपने घर के बिगड़ते रिश्ते को आपस में जोड़ने का काम करती है। कहानी की मुख्य नायिका आनंदी एक बड़े रियासतदार की बेटी है, जिसकी शादी एक जमींदार के घर श्री कंठ सिंह से हो जाती है। आनंदी जितने बड़े घर की बेटी है, उतनी ही सुंदर और सुशील तथा संस्कारों से परिपूर्ण है। वह अपनी समझदारी से अपने घर के बिगड़ते रिश्ते को फिर से बहाल करा देती है। इस कहानी के माध्यम से प्रेमचंद ने यह बतलाने की कोशिश की है कि घर में पारिवारिक शांति और सामंजस्य बनाए रखने में घर की स्त्रियों की भूमिका अहम होती है।
जबकि ‘प्रायश्चित’ एक व्यंग मूलक कहानी है, जिसमें सामाजिक पात्रों की स्वार्थबद्धता पर विनोदपूर्ण और चुटीला व्यंग किया गया है। कथा सम्राट प्रेमचंद का कहना था कि साहित्यकार देशभक्ति और राजनीति के पीछे चलने वाली सच्चाई नहीं बल्कि उसके आगे मशाल दिखाते हुए चलने वाली सच्चाई है। उनके द्वारा लिखे गए 15 उपन्यासों में से ‘गोदान’ कालजयी रचना सिद्ध हुई। प्रेमचंद के उपन्यास न केवल हिंदी उपन्यास साहित्य में बल्कि संपूर्ण भारतीय साहित्य में नील के पत्थर हैं।
उनका पहला उर्दू उपन्यास ‘अशरारे मआविद’ उर्फ ‘देवस्थान रहस्य’ तथा पहला हिंदी उपन्यास ‘सेवा सदन’ है। सेवा सदन में एक नारी के वैश्या बनने की कहानी है। इस उपन्यास के माध्यम से भारतीय नारी की पराधीनता को उजागर किया गया। किसानी जीवन पर लिखा गया उनका पहला उपन्यास प्रेम आश्रम है जो अवध के किसान आंदोलनों के दौरान लिखा गया है। इसके अतिरिक्त ‘रंगभूमि’, ‘कायाकल्प’, ‘निर्मला’, ‘गबन’, ‘कर्मभूमि’, ‘प्रतिज्ञा’, ‘मनोरमा’ आदि इनके द्वारा लिखा गया प्रमुख उपन्यास है।
प्रेमचंद के उपन्यासों का मूल कथ्य भारतीय ग्रामीण जीवन था। प्रेमचंद ने हिंदी उपन्यास को जो ऊंचाई प्रदान की, वे बाद में आने वाले उपन्यासकारों के लिए एक चुनौती बनी रही। उनका सर्वाधिक प्रसिद्ध एवं चर्चित उपन्यास ‘गोदान’ को कई भाषाओं में अनुवादित किया गया। गोदान का हिंदी साहित्य ही नहीं बल्कि विश्व साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। इसमें प्रेमचंद के साहित्य संबंधी विचारधारा आदर्शउन्मुख यथार्थवाद से आलोचनात्मक यथार्थवाद तक की पूर्ण करती है। सामंतवाद और पूंजीवाद के चक्र में फस कर होरी की मृत्यु पाठकों के जहन को झकझोर कर रख देती है।
8 अक्टूबर 1936 को उनकी मृत्यु हो गई और इस तरह से जलता हुआ दीपक सदा के लिए बुझ गया। उन्होंने जीवन भर अपनी ज्ञान की बत्ती जलाकर हिंदी साहित्य का पथ आलोकित किया।
उनका जीवन सरल एवं सादा था। वह विषमताओं से भरे अपने जीवन में सदा हंसमुख रहते थे। सरलता सौजन्यता पर उदारता के वह प्रतिमूर्ति थे। उनके हृदय में एक तरफ जहां मित्रों के लिए उदार भाव था वहीं दूसरी तरफ गरीबों एवं पीड़ितों के लिए सहानुभूति का अथाह सागर था।